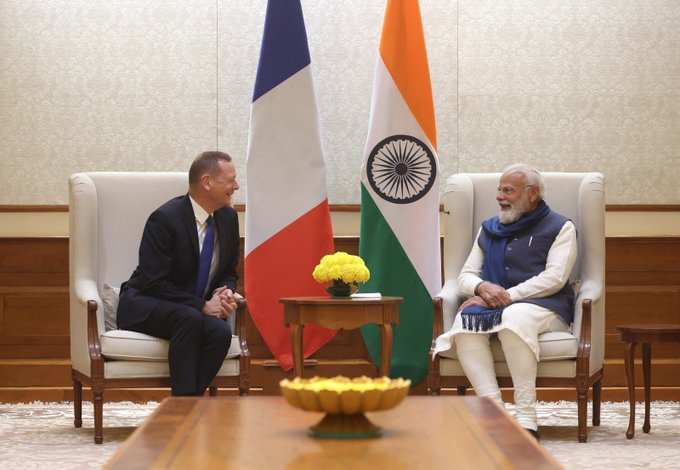लोकतंत्र का ‘महापर्व’ और ‘सलीब’ पर टंगा लोक


योगेश भट्ट
वरिष्ठ पत्रकार
आम चुनाव, कहने को लोकतंत्र का महापर्व । न जाने कैसा महापर्व है यह ? जिसमें तंत्र तो उत्सव में लीन होता है, मगर लोक ‘सलीब’ पर टंगा होता है। आम लोक की तो छोड़िये इस महापर्व में अब तो सियासी दलों का झंडा डंडा उठाने वाले आम राजनैतिक कार्यकर्ता की भी कोई अहमियत नहीं रह गयी है।
राजनैतिक दलों से मोटी रकम लेकर जनमत तैयार करने का काम चुनाव प्रबंधन करने वाली इवेंट मैनेजमेंट और सोशल मीडिया कंपनियां कर रही हैं। कभी जो चुनावी नारे और भाषण आम जनता के बीच से निकल कर आते थे वो भी अब खरीदे हुए होते हैं ।
इन दिनों उत्तराखंड समेत पांच राज्यों में विधानसभा के आम चुनाव होने जा रहे हैं, इन राज्यों में चुनाव से पहले मचा सियासी घमासान किसी से छिपा नहीं है। नेताओं का दलबदल, टिकटों की मारामारी, विद्रोह, टिकट की खरीद फरोख्त, प्रलोभन, बगावत।
बीते एक महीने में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश समेत सभी चुनावी राज्यों में जो जो घटित हुआ उससे यह तो साफ है कि सियासत का कोई धर्म नहीं, सियासत न मूल्यों की है न विचार और सेवाभाव की।
सियासत तो सिर्फ सत्ता और कुर्सी की है । सियासत मुददों की नहीं स्वार्थ, कपट, धनबल और बाहुबल की है । सियासत धर्म और जाति की है। जिस तरह पांच साल तक मंत्री विधायक रहे मंत्रियों की संपत्ति और बैंक बैलेंस में पचास गुना इजाफा हुआ है, उससे यह भी स्पष्ट होता है कि मौजूदा सियासत बड़े मुनाफे का करोबार है।
पांच राज्यों में हालिया विधानसभा आम चुनाव के बहाने ही सही यह चर्चा तो होनी ही चाहिए कि क्या यह आम चुनाव वाकई लोकतंत्र के लिए है । चर्चा से पहले आइये जरा हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक फैसले के दौरान की गयी लोकतंत्र का मंदिर कही जाने वाली संसद और विधानसभा पर की गयी एक टिप्पणी पर गौर करते हैं ।
सुप्रीम कोर्ट का मत है कि संसद और विधानसभा अधिक संवेदनहीन स्थान बनते जा रहे हैं ,अब इनके वैभव को बहाल करने का समय आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह मत महाराष्ट्र विधानसभा से भाजपा के 12 विधायकों को एक वर्ष के निलंबित किए जाने के निर्णय को असंवैधानिक करार देते हुए दिया।
विधानसभा अध्यक्ष के निर्णय को निरस्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि जैसे न्यायपालिका को न्याय का मंदिर माना जाता है वैसे ही संसद और विधानसभसा के सदन को पवित्र स्थान माना जाता है । यही वह पहला स्थल है जहां लोकतांत्रिक प्रक्रिया द्वारा आम आदमी को न्याय मिलता है । यहां मजबूत और निष्पक्ष बहस और चर्चाएं होनी चाहिए ।
लोकतंत्र के आलोक में देखा जाए तो देश की शीर्ष अदालत की यह टिप्पणी बेहद गंभीर है। देश में लोकसभा और राज्यों में विधानसभा के चुनाव के दौरान होने वाली सियासत इसका उदाहरण है कि हमारे यहां लांकतांत्रिक व्यवस्था संस्थागत रूप में ध्वस्त होती चली जा रही है । लोकतंत्र व्यवहार में तो कहीं रह ही नहीं गया है ।
अपने यहां जिन राजनैतिक दलों पर इसे व्यवहार में लाने की जिम्मेदारी है । उनमें या तो तानाशाही है या वह वंशवाद के शिकार हैं । दोनो ही प्रवृतियां लोकतंत्र के लिए घातक हैं । फ्रीडम हाउस संस्था के मुताबित दुनिया के 73 देशों में लोकतंत्र कमजोर पडता जा रहा है । जिसमें सबसे पुराना लोकतंत्र अमेरिका और सबसे बडा लोकतंत्र भारत दोनो ही शामिल हैं ।
दरअसल लोकतंत्र सिर्फ अवधारणा ही नहीं बल्कि एक ऐसी व्यवस्था है, जिसमें लोक और तंत्र के बीच एक बुनियादी रिश्ता होता है। सच्चाई यह है कि जिस व्यवस्था की बुनियाद वंशवादी दलों, आलाकमान के थोपे गए उम्मीदवारों और काले धन पर वह टिकी हो उसमें किसी बुनियादी रिश्ते की उम्मीद कैसे की जा सकती है ?
रहा सवाल फौरी व्यवस्था में आम चुनाव का तो वह रोजी रोटी जुटाने की जुगत में लगे आम आदमी के लिए एक ‘महामारी’ की तरह है । जो तय समय अंतराल पर सियासी दलों के दावों, वायदों और नेताओं के प्रलोभनों के साथ आती है मतदान के साथ ही खत्म हो जाती है।
आम आदमी को कोई सरोकार नहीं कि किसने सरकार बनायी और कौन नाकाम रहा । सरोकार हो भी क्यों ? आम चुनाव के बाद भी न आम आदमी के हालात बदलते हैं और न सियासत का चाल चरित्र। लोक सरोकार तो तब होता जब सरकार के केंद्र में लोक होता। जिस लोकतांत्रिक सरकार को चुनने के लिए आम चुनाव होते हैं , उसके केंद्र में लोक तो कहीं है ही नही।
सरकार भले ही जनता के लिए और जनता के द्वारा हो, मगर जनता की न उम्मीदवार चयन में भागेदारी है न सरकार बनाने में कोई भूमिका। किसे मुख्यमंत्री या मंत्री होना चाहिए यह तय करने का अधिकार तो दूर की बात है। सियासी दलों राज्य और जिले स्तर पर उनका नेतृत्व कौन करेगा यह अधिकार तक आम कार्यकर्ता के पास नहीं है ।
स्पष्ट है कि जो राजनैतिक दल लोकतंत्र को मजबूत करने का झंडा उठाए हुए हैं खुद उनके यहां आंतरिक लोकतंत्र नहीं है । राजनैतिक दल पूरी तरह तानाशाही या फिर वंशवाद से ग्रसित हैं । देश में कोई भी राजनैतिक दल ऐसा नहीं है जहां उम्मीदवार के चयन पर कोई पारदर्शी व्यवस्था हो ।
राजनैतिक दलों की ओर से चुनाव में उतारे गए अधिकांश उम्मीदवार थोपे गए होते हैं। उम्मीदवारी में योग्यता, व्यवहार, राजनैतिक विचारधारा और सामजिक सरोकारों के प्रति निष्ठा, सामाजिक छवि, कर्मठता और चरित्र कोई मायने नहीं रखता । राजनैतिक दलों में उम्मीदवारी कैसे तय होती है, यह भी किसी से छिपा नहीं है ।
राजनैतिक दलों का उम्मीदवार होने के लिए किसी बड़े नेता का कृपा पात्र होना और साधन संपन्न होना अनिवार्य योग्यता है तो किसी राजनैतिक परिवार का सदस्य होना अधिमानी । सालों तक दल की विचारधारा से जुडे कार्यकर्ताओं की भावनाओं और उनके समर्पण के कोई मायने नहीं। चुनाव में उम्मीदवार चयन में उनकी कोई भूमिका नहीं होती ।
अब बताइये जब हाईकमान या सुप्रिमो ने ही सब तय करना है तो फिर किस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं हम ?
लोकतंत्र होता तो उम्मीदवार के चयन का अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिया जाता । पार्टी के कार्यकर्ता बहुत या सर्वसम्मति के आधार पर तय करते कि किस क्षेत्र से कौन चुनाव में उम्मीदवार होगा । बहुमत में आने पर हाईकमान नहीं बल्कि पार्टी के विधायक तय करते कि कौन मुख्यमंत्री होगा ।
लोकतंत्र होता तो सरकार लोक से जुड़े फैसलों में जनसहभागिता सुनिश्चित करती । लोकतंत्र होता तो सरकारें निरंकुश नहीं होती, विपक्ष कमजोर और समर्पण की मुद्रा में नहीं होता । लोकतंत्र होता तो नेता पांच साल सत्ता की मलाई चाटने के बाद ठीक आम चुनाव के वक्त दलबदल नही कर रहे होते ।
टिकट हासिल करने या सत्ता में हिस्सेदारी के लिए राजनेता रातोंरात एक राजनैतिक विचारधारा से कटकर दूसरी विचारधारा का गुणगान नहीं कर रहे होते । लोकतंत्र होता तो सियासत चंद नेताओं की जागीर नहीं होती । चंद राजनेता ही सियासत को विरासत मान अपनी बेटी, बेटे या पत्नि, बहु को सौंपने की कल्पना नहीं करते।
सही मायने में अगर लोकतंत्र होता तो कोई राजनैतिक दल जनता को मुफतखोर समझ वोट के एवज में मुफत बिजली, मुफत लैपटाप या फिर खाते में चंद रुपयों की पेशकश नही कर पाते । आम चुनाव वाले राज्यों में जरा एक नजर दौड़ाईये, देखिए अभी पिछले दिनों क्या हुआ ?
वर्षों तक एक राजनैतिक विचारधारा के साथ जुडकर संगठन और सरकार में अहम पदों पर रहने वाले कई राजनेताओं ने दलबदल किया । दिलचस्प यह है कि ठीकि चुनाव से पहले इसके लिए जनता की आड़ ली गयी, पांच साल तक श्रम और रोजगार मंत्री रहने के बाद यूपी में स्वामी प्रसाद मौर्य और उत्तराखंड में हरक सिंह यह कहते हुए पाला बदल डालते हैं कि बेरोजगारों के साथ अन्याय हो रहा था ।
तमाम राजनैतिक दल भी रेड कार्पेट बिछाकर दलबदल को बढ़ावा दे रहे हैं। यह आंकलन तक नहीं किया जा रहा है दलबदल से क्या नुकसान होने जा रहा है । यह जानना भी जरूरी नहीं समझा जा रहा है कि ठीक चुनाव से पहले दलबदल क्यों ? हकीकत में कोई भी दलबदल देश, प्रांत, शहर अथवा निर्वाचन क्षेत्र विशेष के फायदे के लिए नहीं होता । सामाजिक, राजनैतिक मूल्यों की रक्षा के लिए भी कोई दलबदल नहीं करता । दलबदल होता है सिर्फ निजी स्वार्थ के लिए ।
जब किसी को अपनी सियासत के सिमटने का भय होता है या सत्ता से बेदखल होने की आशंका होती तब दलबदल होता है। जब किसी को अपनी सीट बदलनी होती है या किसी को अपने बेटी, बहू, भाई, बेटे और पत्नि को मनमानी सीट दिलानी होती है तब दलबदल होता है।
दलबदल के बाद आम चुनाव चंदे की रकम से नहीं काले धन से लड़े जाते हैं । तय सीमा से कई गुना अधिक ज्यादा चुनावों में खर्च किया जाता है । ऐसी प्रवृति से अक्सर चुनाव इतना मंहगा हो जाता है कि एक सामान्य सामाजिक कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के विषय में सोच भी नहीं सकता ।
अंततः इस पूरी प्रक्रिया में नुकसान राजनैतिक दलों का नहीं,लोकतंत्र की अवधारणा और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूती देने वाली राजनीति को नुकसान पहुंच रहा है । यही विचारणीय भी है कि राजनीति जब विचारधारा और मूल्यों से हटकर सिर्फ सत्ता केंद्रित होकर रह जाएगी तो लोकतंत्र कैसे सुरक्षित होगा ?
इसी कड़ी में एक विचारणीय तथ्य यह भी है कि हम अपने यहां निष्पक्ष और स्वतंत्र आम चुनाव का दावा करते हैं, लेकिन चुनाव प्रक्रिया की सच्चाई यह है कि जिसमें औसतन तीस से तैतीस फीसदी मतदाता ही सौ फीसदी मतदाताओं का भाग्य तय कर देते हैं। आबादी के लिहाज से देखें तो यह आंकडा बामुश्किल पच्चीस फीसदी भी नहीं बैठता।
जरा सोचिए ऐसे में लोक और तंत्र के बीच का कोई रिश्ता कैसे कायम रह सकता है ? आज जरूरत यह विचार करने की है कि निष्पक्ष और स्वतंत्र आम चुनाव कराने का दावा करने वाले देश में ऐसी स्थिति क्यों है ?
दरअसल लोक और तंत्र के रिश्ते को बनाए रखने के लिए सिर्फ निष्पक्ष आम चुनाव के दावे ही काफी नहीं है । लोकतंत्र को बचाना है, उसे मजबूत करना है तो सबसे पहले राजनैतिक दलों को अपने यहां आंतरिक लोकतंत्र स्थापित करना होगा।
इसके लिए सिर्फ राजनैतिक दलों को ही नहीं बल्कि आम राजनैतिक कार्यकर्ताओं के साथ लोक को भी गंभीर होना पड़ेगा । इतना ही नहीं, मतदान को अनिवार्य कराते हुए सभी को एकसाथ चुनाव सुधार पर जोर देना होगा ।
आम चुनाव संपन्न करानी वाली संस्था केंद्रीय चुनाव आयोग से चुनाव सुधार की बातें समय समय पर उठती तो हैं, मगर चुनाव आयोग की अपनी सीमा है। लोक और तंत्र के बीच रिश्ता कायम रहे इसके लिए चुनाव आयोग का अधिकार संपन्न होना बहुत जरूरी है।
देश के राजनैतिक दल और आम जनता अगर लोकतंत्र के प्रति ईमानदार है पूरी इच्छाशक्ति के साथ चुनाव आयोग को चुनाव के वक्त दलबदल रोकने, काले धन से चुनाव लड़ने लड़ाने, वोट के लिए किसी भी तरह के प्रलोभन दिये जाने या चुनाव घोषणा पत्रों में किसी भी तरह की मुफत पेशकश पर रोक लगाने के अधिकार दिये जाने की पैरवी करनी होगी ।
जिस दिन धनबल और बाहुबल के दम पर सियासत में घुसपैठ करने वालों में चुनाव आयोग का खौफ पैदा होगा सही मायने में उस दिन लोकतंत्र मजबूत होगा। निसंदेह चुनाव आयोग जितना निष्पक्ष और अधिकार संपन्न होगा, लोक और तंत्र के बीच का रिश्ता भी उतना ही गहरा होगा । सनद रहे कि जब सलीब टंगा लोक आम चुनाव के केंद्र में होगा तभी सही मायनों में आम चुनाव लोकतंत्र का ‘महापर्व’ कहलाएगा ।
फेसबुक पोस्ट से साभार…