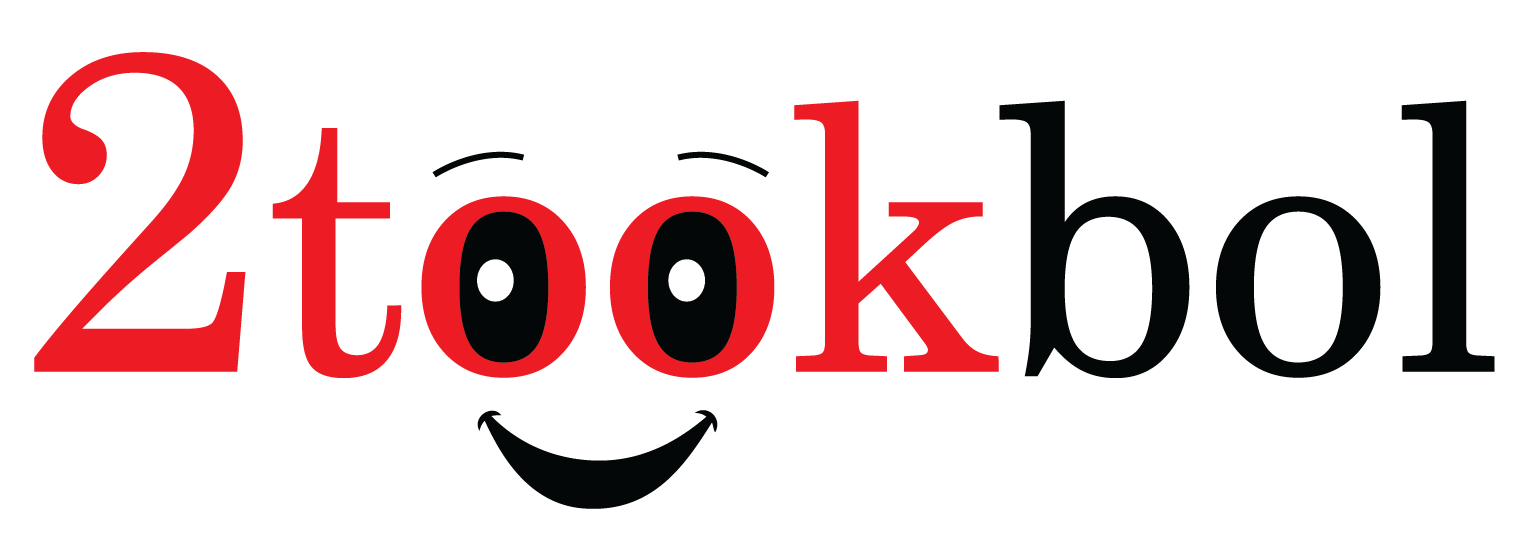विशेष : मेक इन इंडिया और कैपिटल गुड्स की क्रांति

घरेलू उत्पादन और तकनीकी नवाचार का उत्प्रेरण
नई दिल्ली : भारत की कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री औद्योगिक विकास और आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण काफी ध्यान आकर्षित कर रही है। इस क्षेत्र में विद्युत उपकरण, मशीनरी और निर्माण जैसे कारोबार शामिल हैं, जो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए जरूरी हैं। भारतीय विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता संघ (आईईईएमए) के अनुसार, विद्युत उपकरण उद्योग ने घरेलू मांग और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के विस्तार से प्रेरित होकर ऊर्जा उपकरणों, विशेष रूप से ट्रांसमिशन उपकरण और ट्रांसफार्मर में लगातार दोहरे अंकों की बढ़ोतरी देखी।
भारत निर्माण उपकरणों का तीसरा सबसे बड़ा बाजार है। पूंजीगत सामान क्षेत्र को मजबूत करने में सरकारी पहलों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारी उद्योग मंत्रालय ने घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहन देने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए कई नीतियां शुरू की हैं। ये पहल व्यापक मेक इन इंडिया अभियान (2014 में शुरू) का हिस्सा हैं, जिसका उद्देश्य सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान बढ़ाना, रोजगार पैदा करना और तकनीकी क्षमताओं में सुधार करना है। कैपिटल गुड्स सेक्टर भारत की आर्थिक रणनीति के लिए महत्वपूर्ण है, जो बड़े पैमाने पर विनिर्माण और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में सहयोग करता है। तेजी से शहरीकरण, व्यापक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और मजबूत सरकारी सहयोग के साथ, यह क्षेत्र संपोषित औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देने और वैश्विक बाजार में भारत की स्थिति को बेहतर करने के लिए तैयार है। भारी उद्योग मंत्रालय के अनुसार, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री में भारी इंजीनियरिंग और मशीन टूल्स क्षेत्र शामिल हैं।
भारी उद्योग और अभियांत्रिकी क्षेत्र का अवलोकन
हालिया अनुमानों के अनुसार, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री जीडीपी में लगभग 1.9% का योगदान देती है। भारी इंजीनियरिंग और मशीन टूल सेक्टर (कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री) में निम्नलिखित प्रमुख उप-क्षेत्र: डाई, मोल्ड्स और प्रेस टूल्स; प्लास्टिक मशीनरी; अर्थमूविंग और माइनिंग मशीनरी; धातुकर्म मशीनरी; कपड़ा मशीनरी; प्रोसेस प्लांट उपकरण; प्रिंटिंग मशीनरी; और खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी शामिल हैं। भारी उद्योग मंत्रालय के सहयोग के उत्प्रेरक प्रभाव के चलते, कैपिटल गुड्स सेक्टर का उत्पादन 2014-15 में 2,29,533 करोड़ रुपये से बढ़कर 2023-24 में 4,29,001 करोड़ रुपये हो गया है।
कैपिटल गुड्स सेक्टर के लिए नीतिगत परिवेश में निम्नलिखित शामिल हैं:
इस क्षेत्र के लिए किसी औद्योगिक लाइसेंस की जरूरत नहीं है।
भारत के साथ भूमिगत सीमा वाले देशों को छोड़कर, स्वचालित मार्ग (आरबीआई के जरिए) पर 100% तक एफडीआई की अनुमति है।
विदेशी सहयोगी को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, डिजाइन और ड्राइंग, रॉयल्टी आदि के लिए भुगतान की मात्रा सीमित नहीं है।
आयात और निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
केंद्रीय बजट 2025-26 में छूट प्राप्त पूंजीगत वस्तुओं की सूची में ईवी बैटरी निर्माण के लिए 35 अतिरिक्त पूंजीगत वस्तुओं और मोबाइल फोन बैटरी निर्माण के लिए 28 अतिरिक्त पूंजीगत वस्तुएं शामिल करने का प्रस्ताव है। इससे मोबाइल फोन और इलेक्ट्रिक वाहनों दोनों के लिए लीथियम-आयन बैटरी के घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा।
राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति (2016)
भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय की ओर से तैयार की गई राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति, भारत में कैपिटल गुड्स सेक्टर को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से एक व्यापक रूपरेखा है। नीति में विनिर्माण गतिविधि में इस क्षेत्र के योगदान को 12% (2016) से बढ़ाकर 2025 तक 20% करने की परिकल्पना की गई है। यह भारत को शीर्ष पूंजीगत वस्तु उत्पादक देशों में से एक बनाने का प्रयास करती है, जिसका लक्ष्य उत्पादन को दोगुने से अधिक करना और निर्यात को कुल उत्पादन का कम से कम 40% तक बढ़ाना है। इसके अतिरिक्त, नीति का उद्देश्य इस क्षेत्र के भीतर प्रौद्योगिकी की गहराई को बढ़ाना है, जो बुनियादी और मध्यवर्ती स्तरों से उन्नत स्तरों तक ले जाएगा।
नीति की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:
कैपिटल गुड्स सेक्टर में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने की योजना के बजटीय आवंटन और दायरे को बढ़ाना, जिसमें कौशल, क्षमता निर्माण, उन्नत विनिर्माण और क्लस्टर विकास जैसे घटक शामिल हैं।
प्रौद्योगिकी अधिग्रहण/ हस्तांतरण, बौद्धिक संपदा अधिकारों की खरीद/ डिजाइन और रेखाचित्र/ व्यावसायीकरण के लिए पीपीपी मॉडल के अंतर्गत प्रौद्योगिकी विकास निधि शुरू करना।
कौशल विकास के लिए क्षेत्रीय अत्याधुनिक ग्रीनफील्ड उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करना।
पूंजीगत वस्तु उप-क्षेत्रों में, कंप्यूटर नियंत्रित और ऊर्जा कुशल मशीनरी के साथ मौजूदा आधुनिक सीजी विनिर्माण इकाइयों, विशेष रूप से एसएमई का आधुनिकीकरण करना।
परीक्षण और प्रमाणन बुनियादी ढांचे को उन्नत/ तैयार करना।
राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति, 2016 में अन्य बातों के साथ-साथ पूंजीगत वस्तुओं की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने की योजना के बजटीय आवंटन और दायरे को बढ़ाने की सिफारिश की गई थी, जिसमें उत्कृष्टता केंद्र, सामान्य इंजीनियरिंग सुविधा केंद्र, एकीकृत औद्योगिक अवसंरचना पार्क और प्रौद्योगिकी अधिग्रहण निधि कार्यक्रम की स्थापना शामिल थी। इन सिफारिशों को योजना के चरण II में शामिल किया गया था।
भारत के कैपिटल गुड्स सेक्टर में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने की योजना का चरण I
कैपिटल गुड्स सेक्टर के लिए कौशल अंतराल, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और प्रौद्योगिकी की जरूरतों को पूरा करने के लिए, पूंजीगत वस्तु योजना का चरण I नवंबर 2014 में शुरू किया गया था, जिसका कुल आउटले 995.96 करोड़ रुपये था। योजना के पहले चरण में सरकारी सहायता से प्रौद्योगिकी विकास को प्रोत्साहन देने के लिए शिक्षाविदों और उद्योग के बीच साझेदारी को बढ़ावा दिया गया। योजना के परिणामों ने प्रौद्योगिकी और औद्योगिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अपनाई गई रणनीतियों के प्रभाव को सिद्ध कर दिया है।
उत्कृष्टता केंद्र (सीओई): 8 सीओई स्थापित किए गए हैं, जिनमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी), केंद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान (सीएमटीआई) आदि जैसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थानों में मशीन टूल्स, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल मशीनरी, वेल्डिंग रोबोट और मिश्र धातु डिजाइन, अर्थ मूविंग मशीनरी और सेंसर प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में 30 विशिष्ट स्वदेशी प्रौद्योगिकियों को सफलतापूर्वक तैयार किया गया है।
सामान्य इंजीनियरिंग सुविधा केंद्र (सीईएफसी) – चार इंडस्ट्री 4.0 समर्थ केंद्रों और छः वेब-आधारित प्रौद्योगिकी नवाचार प्लेटफॉर्म (टीआईपी) सहित 15 सीईएफसी स्थापित किए गए हैं। इंडस्ट्री 4.0 समर्थ केंद्र बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान, पुणे में इंडस्ट्री 4.0 (सी4आई4) प्रयोगशाला केंद्र, बेंगलुरु में केंद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान (सीएमटीआई) और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) दिल्ली में हैं।
छः वेब-आधारित ओपन विनिर्माण प्रौद्योगिकी नवाचार मंच भारत के सभी तकनीकी संसाधनों और संबंधित उद्योग को एक मंच पर लाने में मदद कर रहे हैं, ताकि भारतीय उद्योग के सामने आने वाली प्रौद्योगिकी समस्याओं की पहचान और उनके लिए व्यवस्थित तरीके से क्राउड सोर्स समाधान की सुविधा मिल सके, जिससे स्टार्ट-अप और भारत के नवाचारों के लिए एंजल फंडिंग की सुविधा मिल सके।
अब तक 76,000 से अधिक छात्र, विशेषज्ञ, संस्थान, उद्योग और प्रयोगशालाएं इन प्लेटफार्मों पर पंजीकरण करा चुके हैं।
प्रौद्योगिकी अधिग्रहण निधि कार्यक्रम (टीएएफपी) – टीएएफपी के अंतर्गत विदेशों से निम्नलिखित 5 प्रौद्योगिकियां प्राप्त की गई हैं:
सिरेमिक शेलिंग प्रौद्योगिकी के साथ टाइटेनियम कास्टिंग का विकास और व्यवसायीकरण;
हैवी-ड्यूटी उच्च विश्वसनीयता वाले विद्युत विशेषीकृत पावर केबल्स का विनिर्माण;
टर्न मिल सेंटर का विकास;
चार गाइडवे सीएनसी खराद का विकास;
कटिंग एज रोबोटिक लेजर क्लैडिंग प्रौद्योगिकी।
एकीकृत मशीन टूल्स पार्क, तुमकुरु: कर्नाटक के तुमकुरु में 530 एकड़ में मशीन टूल उद्योग के लिए एक विशेष औद्योगिक पार्क तैयार किया गया है। अब तक, आवंटन योग्य 336 एकड़ भूमि में से, 145 एकड़ भूमि मशीन टूल निर्माताओं को आवंटित की गई है।
भारतीय कैपिटल गुड्स सेक्टर में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने की योजना के चरण-I के अंतर्गत, 583.312 करोड़ रुपये के बजटीय सहयोग के साथ 33 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। पूंजीगत वस्तु योजना चरण II के शुभारंभ के बाद, पूंजीगत वस्तु योजना के चरण I को योजना के चरण II के साथ मिला दिया गया है।
भारतीय कैपिटल गुड्स सेक्टर में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने की योजना चरण II
भारी उद्योग मंत्रालय ने 25 जनवरी, 2022 को योजना के चरण II को अधिसूचित किया, जिसका उद्देश्य पूंजीगत वस्तु योजना के पहले चरण I द्वारा सृजित प्रभाव को विस्तारित और व्यापक बनाना है, जिससे एक सुदृढ़ और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी कैपिटल गुड्स सेक्टर के निर्माण के माध्यम से अधिक प्रोत्साहन मिल सके। इस योजना का वित्तीय आउटले 1207 करोड़ रुपये है, जिसमें 975 करोड़ रुपये का बजटीय सहयोग और 232 करोड़ रुपये का उद्योग का योगदान शामिल है। दूसरे चरण के अंतर्गत, अगस्त 2024 तक 1366.94 करोड़ रुपये (उद्योग द्वारा अधिक योगदान के कारण) की परियोजना लागत और 963.19 करोड़ रुपये के सरकारी योगदान वाली कुल 33 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। दूसरे चरण के तहत छः घटक हैं और अब तक स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण इस प्रकार है:
नए उन्नत उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना और मौजूदा उत्कृष्टता केंद्रों का विस्तार: अनुसंधान और विकास गतिविधियों में शामिल प्रतिष्ठित शिक्षाविदों और निजी उद्योग का उपयोग करके अनुसंधान और विकास में तेजी लाना। अब तक 478.87 करोड़ रुपये के बजट वाली कुल 9 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।
सामान्य इंजीनियरिंग सुविधा केंद्रों (सीईएफसी) की स्थापना और मौजूदा सीईएफसी का विस्तार: औद्योगिक इकाइयों के लिए प्रदर्शन और प्रशिक्षण, सलाह, सहायता और अनुसंधान एवं विकास सेवाएं तथा जागरूकता कार्यक्रम बनाना। अब तक 357.07 करोड़ रुपये के बजट वाली कुल 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।
कैपिटल गुड्स सेक्टर में कौशल को प्रोत्साहन: कौशल स्तर 6 और उससे ऊपर के लिए कौशल परिषदों के सहयोग से योग्यता पैकेजों का निर्माण। अब तक 7.59 करोड़ रुपये के बजट वाली कुल 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।
मौजूदा परीक्षण और प्रमाणन केंद्रों का विस्तार: मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, स्ट्रक्चरल, मेटलर्जिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि पहलुओं से संबंधित विभिन्न गुणों के संदर्भ में मशीनरी के परीक्षण के लिए कैपिटल गुड्स सेक्टर और ऑटो क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करना। अब तक 195.99 करोड़ रुपये के बजट वाली कुल 7 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।
प्रौद्योगिकी विकास के लिए उद्योग एक्सेलेटर्स की स्थापना: इसका उद्देश्य लक्षित स्वदेशी प्रौद्योगिकियों का विकास करना है, जो चयनित उद्योग क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हैं, जो अब तक आयात पर निर्भर रहे हैं। चयनित शैक्षणिक संस्थान/ उद्योग निकाय ऐसी प्रौद्योगिकियों के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए एक्सेलेटर के तौर पर कार्य करेंगे। अब तक 325.32 करोड़ रुपये के बजट वाली कुल 8 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।
प्रौद्योगिकी नवाचार पोर्टल के माध्यम से प्रौद्योगिकियों की पहचान: सीजी योजना चरण-I के अंतर्गत छः वेब-आधारित ओपन मैन्युफैक्चरिंग प्रौद्योगिकी नवाचार प्लेटफॉर्म तैयार किए गए हैं। इन्हें सीजी योजना चरण-II के तहत सहयोग किया जा रहा है।
भारतीय कैपिटल गुड्स सेक्टर में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने की योजना के चरण-I और II के अंतर्गत आवंटित धनराशि और इसके इस्तेमाल का विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:
कैपिटल गुड्स स्कीम की वर्तमान में उपलब्धियां
सिटार्क, कोयंबटूर ने कैपिटल गुड्स स्कीम के अंतर्गत स्वदेशी रूप से 6-इंच का बीएलडीसी सबमर्सिबल पंप तैयार किया है, जिसकी मोटर दक्षता 88% और पंप दक्षता 78% है। यह पहल ऐसे पंपों के आयात को 80% तक कम करके “आत्मनिर्भरता” को प्रोत्साहन देती है। इस नवाचार को संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (यूएनआईडीओ) की ओर से पंप श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ उत्पाद के रूप में मान्यता दी गई थी।
सीएमटीआई ने 450 आरपीएम तक यार्न बुनाई में सक्षम एक हाई-स्पीड रैपियर लूम मशीन तैयार की है। इस मशीन को इटली के मिलान में आईटीएमए 2023 में लॉन्च किया गया था।
सीएमटीआई में समर्थ केंद्र के अंतर्गत, निवारक रखरखाव के लिए 64 मशीनों को नियंत्रित करने वाली टोयोटा इंजन मैन्युफैक्चरिंग लाइन में औद्योगिक इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईआईओटी) तकनीक लागू की गई है।
भारी उद्योग मंत्रालय के तत्वावधान में भारत में पहली बार एआरएआई, पुणे में बैटरी और बैटरी प्रबंधन प्रणाली (बीएमएस) के लिए एक परीक्षण सुविधा स्थापित की गई है।
आई-4.0 इंडिया @ आईआईएससी, बेंगलुरु में डिजिटल ट्विन, वर्चुअल रिएलिटी, रोबोटिक्स, निरीक्षण, स्थिरता, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग आदि में 6 स्मार्ट टेक्नोलॉजीज, 5 स्मार्ट टूल्स, 14 समाधान तैयार किए गए हैं;
एआरएआई-एडवांस्ड मोबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन फाउंडेशन (एएमटीआईएफ) में इंडस्ट्री एक्सेलेरेटर के अंतर्गत एक हाई-वोल्टेज मोटर कंट्रोलर तैयार किया गया, जिसने इंडस्ट्री पार्टनर रैप्टी एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को इलेक्ट्रिक कार डीएनए के साथ एक हाई-वोल्टेज मोटरसाइकिल लॉन्च करने के योग्य बनाया।
एआरएआई-एडवांस्ड मोबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन फाउंडेशन (एएमटीआईएफ) में इंडस्ट्री एक्सेलेरेटर के अंतर्गत थर्मली स्टेबल सोडियम-आयन बैटरी तैयार की गई।
भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल)
बीएचईएल देश के लिए इंजीनियरिंग और विनिर्माण क्षमता निर्माण में एक प्रमुख योगदानकर्ता है। कंपनी कैपिटल गुड्स योजना चरण II के अंतर्गत भारी उद्योग मंत्रालय के सहयोग से निम्नलिखित पहल कर रही है:
बीएचईएल ने वेल्डिंग प्रौद्योगिकी में कौशल विकास के लिए डब्ल्यूआरआई त्रिची में एक “कॉमन इंजीनियरिंग फैसिलिटी सेंटर (सीईएफसी)” की स्थापना की, साथ ही बीएचईएल की वाराणसी, रानीपेट, भोपाल, झांसी और हरिद्वार इकाइयों में इसके विस्तार केंद्रों की भी स्थापना की है।
बीएचईएल भारी उद्योग मंत्रालय के सहयोग से हैदराबाद में अपनी कॉरपोरेट अनुसंधान एवं विकास इकाई में औद्योगिक, नौसेना और विमान संबंधी प्रक्रियाओं के क्षेत्र में हार्डवेयर इन द लूप (एचआईएल) और सॉफ्टवेयर इन द लूप (एसआईएल) दोनों कार्य करने की क्षमता को शामिल करते हुए एक परीक्षण सुविधा स्थापित कर रहा है।
निष्कर्ष
‘मेक इन इंडिया’ पहल का भारी उद्योगों और इंजीनियरिंग क्षेत्र पर परिवर्तनकारी असर पड़ा है। तकनीकी प्रगति को प्रोत्साहन देकर, घरेलू उत्पादन में बढ़ोतरी करके, प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाकर और रोजगार पैदा करके, इस पहल ने भारत के औद्योगिक आधार को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। निरंतर नीति समर्थन और निरंतर निवेश के साथ, यह क्षेत्र आने वाले वर्षों में और अधिक विकास के लिए तैयार है।